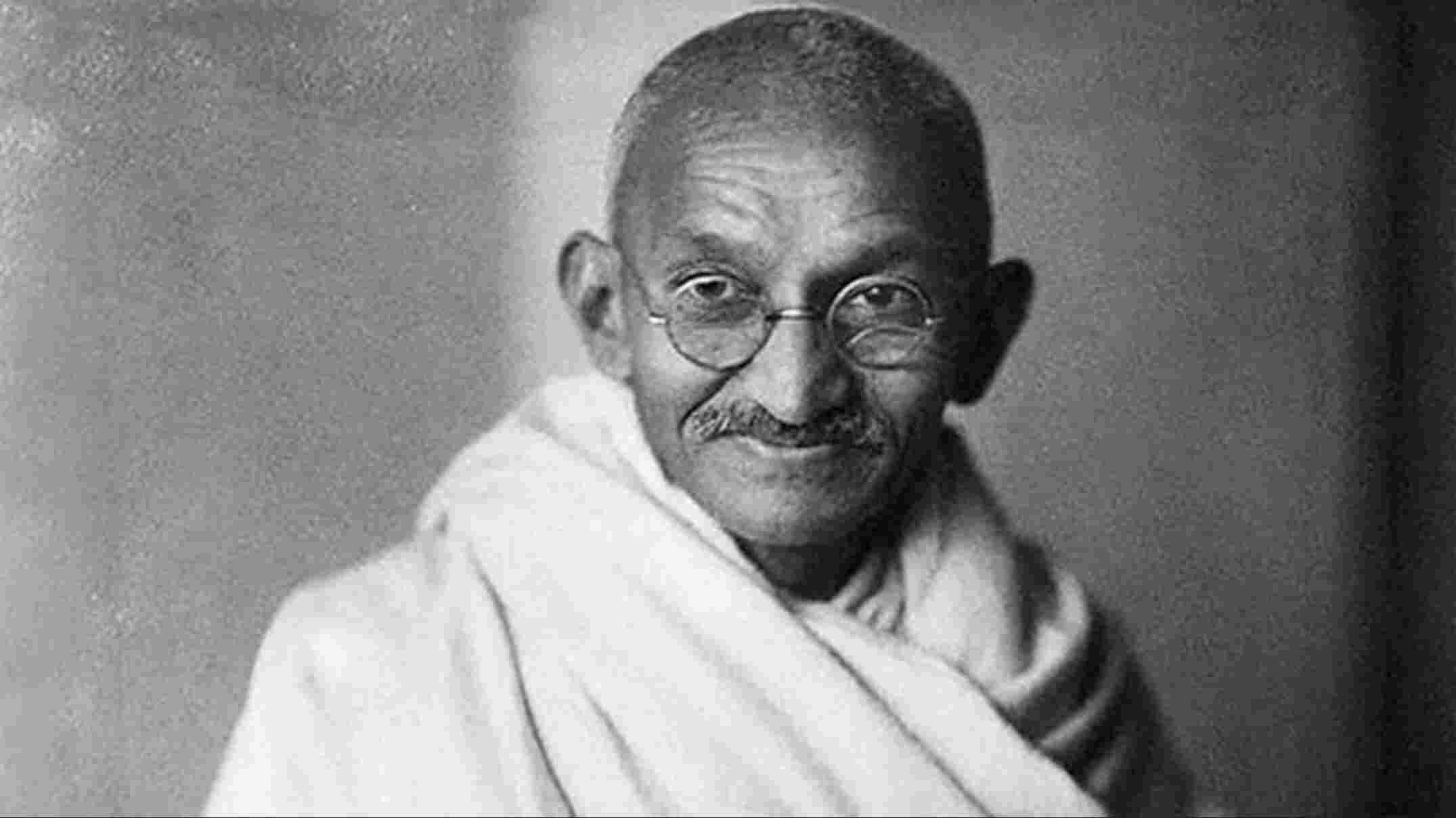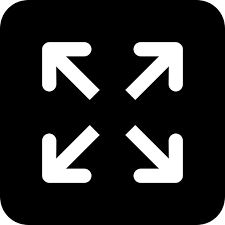जिस तरह निराला ने कविता को छंदों से मुक्त किया, केदारनाथ सिंह ने उदात्तता से मुक्त किया उसी तरह एक हद तक रघुवीर सहाय ने और ज्यादा समर्थ ढंग से विष्णु खरे ने उसे करुणा की अकर्मण्य लय से मुक्त किया है। केदारनाथ सिंह के यहाँ करुणा की जगह अगर खुशी दिखाई देती है, रघुवीर सहाय के यहाँ अगम्य-अवध्य आतंक, तो खरे के यहाँ क्षोभ और यथार्थ का स्वीकार मिलता है।
वरिष्ठ कवि—पत्रकार विष्णु खरे से कुमार मुकुल की बातचीत के अंश
आपकी कविताओं में रूप से ज़्यादा कथ्य पर ज़ोर होता है. रूप या कविता के लिए कविता क्या ज़रूरी है? कविता, कहानी, आलेख में रूप को हटा दिया जाए तो क्या सपाट विचार जीवित नहीं रह सकते?
यदि कोई कवि है तो वह पहले ‘रूप’ ‘कहना’ चाहता है या ‘कथ्य’? पारंपरिक कविता को छोड़ दीजिये जिसमें कवि अपने-अपने पिंगल-शास्त्र या उसके अपने अर्जित ज्ञान और अभ्यास, के अनुसार अपनी उद्दिष्ट कृति के स्वरूप या आकार की ‘कल्पना’ करके चलते हैं. आज का कवि गंभीर प्रयोग या कौतुक के लिए भी गाहे-बगाहे ऐसा कर लेता है. लेकिन कविता पारंपरीण हो या अधुनातन, हर संज़ीदा सुख़नसाज़ शुरू ही कुछ कथ्य से करता है.
जब कोई पंक्ति ज़ेहन और काग़ज़ पर उतरती है तो वह अपनी लय के साथ अपना प्रारंभिक शिल्प और रूप लेती आती है. एक कवि की हैसियत से मुझे पहले यह जानना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और उसके मुताबिक मैं शब्द जुटा पा रहा हूँ या नहीं. अक्सर तो वह कमोबेश अपना रूप साथ ले ही आते हैं, वरना बाक़ी काम आपको काग़ज़ या ‘वर्ड’ पर अंजाम देना होता है. सिद्धांत यह है कि रूप के बिना कथ्य संभव है, कथ्य के बिना कुछ भी संभव – या आवश्यक – नहीं होगा. विचारों को शुद्ध विचारों की तरह जीवित रहने के लिए एक चिंतनशील मस्तिष्क और एक समर्थ भाषा चाहिए.उन्हें किसी ‘रूप’ की दरकार नहीं रहती. 'सपाट’ विचार नामक कोई वस्तु नहीं होती. हज़ारों ‘मामूली’ और ‘रोज़मर्रा’ ख़याल तो हर क्षण आते रहते हैं, किन्तु अनिवार्य होते हुए भी वे चिंतन या सृजन की श्रेणी में नहीं गिने जाएँगे. अलबत्ता कविता का कच्चा माल वह भी बन सकते है.
कविता या कहानी में प्रेमचंद, निराला की परंपरा को आप किस तरह देखते हैं? आप ख़ुद को किस परंपरा में पाते हैं?
आज प्रेमचंद की परंपरा को हिंदी साहित्य में शायद सिर्फ़ एक बची-खुची भारतीय मानवीय प्रतिबद्धता के रूप में ही देखा जा सकता है. सवाल यह भी है क्या कभी प्रेमचंद या दूसरे कुछ हिंदी लेखक पूरे भारत के प्रतिनिधि बन भी पाए थे? 1936 के बाद के इन 80 वर्षों में भारत का सब कुछ कई अवधियों, दौरों और जिन्हें अंग्रेज़ी में fits and starts कहा जाता है, में बदला है. जब आज की परिवर्तनशील दुनिया को समझने के लिए मार्क्सवाद को दोबारा, नए ढंग से पढ़ना होगा तो प्रेमचंद का भारत और उसके बाशिंदे तो अब कुछ और होकर कहीं और जा रहे है.
कुछ दिवास्वप्न देखने या परस्पर विलाप करने के अलावा हम ‘लेखकों-बुद्धिजीवियों’ के पास, जिन्होंने इंदिरा गाँधी के युग से सक्रिय क्रांतिधर्मा राजनीति से लगातार पलायन किया,बचा क्या है? मैं 77 वर्षों से इस देश में हूँ, लेकिन मुझे नरेन्द्र मोदी के भारत को समझने की कोशिश आज रोज़ करनी पड़ती है. इंदिरा गाँधी सहित पिछले सभी प्रधानमंत्रियों के साथ अगल-अलग ढंग से ऐसा करना पड़ा था. विचित्र है कि आज जहाँ प्रेमचंद की सामाजिक परंपरा बहुत कारगर नज़र नहीं आती – बदले हुए भारत में जैनेन्द्र कुछ ज़्यादा प्रासंगिक लगते हैं – वहीं अपनी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अर्ध-प्रतिक्रियावादी कविताओं को छोड़कर निराला अब भी अपनी अनेक रचनाओं में कथ्य और शिल्प-रूप में मुझे-जैसों को अपनी ‘परंपरा’ में खींचते लगते हैं.लेकिन विडंबना है कि प्रेमचंद की भाषा कवियों के लिए भी अब तक अद्वितीय बनी हुई है. रघुवीर सहाय ने उनसे सीखकर हम-जैसों को पट्टी पढ़ाई है.
सोशल मीडिया नई रचनाशीलता को तेजी से प्रभावित कर रहा है, इसको आप कितना सकारात्मक मानते हैं?
जबसे सोच-समझ की थोड़ी क़ूवत आई है देख रहा हूँ कि हिंदी में हर दौर के घटिया नए ‘रचनाशील’ अपने वक़्त के कथित सोशल मीडिया ही नहीं, सारी प्रचलित पिष्टोक्तियों, हर क्षेत्र की फैशनों से अविलम्ब प्रभावित होने की चूहा-दौड़ में नाम लिखाने पहुँच पड़ते हैं. बेशुमार जाहिल युवा-अधेड़ महिला-पुरुष हिंदी ‘लेखक-लेखिकाएँ’ इनमें दर्ज़ हैं – महिलाओं को कृपया कम न समझें. यह ‘लेटेस्ट’ होने का प्रातियोगिक प्रदर्शन-नरक है.
साहित्य अब एक ‘रैंप’, एक रिअलिटी शो भी होता जा रहा है जिसमें प्रायोजित जाँघिया-चोली मासूम सार्वजनिक लापरवाही से उतर जाते हैं. देश या मानवता में जो भी कुछ घट रहा है वह इन पर सिर्फ़ सतही तौर पर ही शुरुआती असर डालता है, लेकिन इन्हें भी उसे फ़ौरन अख़बार के ‘यूज़ एंड थ्रो’ विज्ञापकीय परिशिष्टों के कॉलम या फ़ीचर की तरह भुनाना है. समाज और व्यक्ति को बदलने में अक्सर पर्याप्त देर लगती है और फिर ‘जितना बदलने उतना ही पूर्ववत् होते जाने’ की विडंबना भी सक्रिय होती जाती है. लेकिन कुछ युवा-प्रौढ़ स्त्री-पुरुष प्रतिभाएँ हमेशा होंगीं जो गहरे निरीक्षण और परीक्षण के बाद उसे सार्वजनीन मानवीय ‘फेनोमेनन’ के रूप में प्रस्तुत करने का सर्जनात्मक जोखिम उठाएँगी.
रागात्मक स्वरूप वाली अप्रतिम सौन्दर्यबोध की ‘द्रौपदी के विषय में कृष्ण’ जैसी कविताएँ आपके पास हैं.क्या इसे प्रेम-कविता कहा जा सकता है? कविता के लिए ‘प्रेम’ आदि ‘टैग्स’ को आप कहाँ तक युक्तिसंगत मानते हैं?
मेरी वैसी कविताओं के बारे में आपकी उदार राय से ख़ुद सहमत न होते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरी ही नहीं, बल्कि दूसरों की वैसी रचनाओं के लिए भी उचित लगे तो ‘राग कविता(एँ)’ प्रत्यय प्रयुक्त होना चाहिए – ठीक इसलिए भी कि हिंदी में ‘प्रेम’ वाक़ई एक बदरंग लेबिल बन चुका है जिसे बहुत नोचा-खुरचा गया है. द्रौपदी और कृष्ण के बीच जो जटिल सम्बन्ध द्वापर में थे वह स्त्री-पुरुष के बीच भारत और हिंदी में आज कहीं-कहीं नज़र आते हैं – देखिए जैनेन्द्र - लेकिन विश्व में तो उनका वैविध्य अनंत है.वह प्रेम-सम्बन्ध है या वृहत्तर राग-सम्बन्ध? दरअसल लगभग सभी क्षेत्रों में,व्यक्तियों को लेकर भी, एक अवधि और सीमा के बाद हर ‘टैग’ अपनी पहचान और उपयोगिता खोने को अभिशप्त है.
पत्रकारिता में सुर्ख़ियों में कई सनसनीखेज क्लिशेज़ का इस्तेमाल सिर्फ़ पाठकों को चौंकाने के लिए हो रहा है. कई बार ख़बर के शीर्षक का सम्बन्ध समाचार से होता ही नहीं है.आज की पत्रकारिता की दशा-दिशा पर कुछ कहना चाहेंगे?
मैं स्वयं को हिंदी पत्रकारिता के पाषाणकालीन माथुरैसिक युग के कुछ अंतिम किन्तु माँद में आसरा लिए हुए अपने घाव चाटते डाईनोसॉरों में देखता हूँ. उस ज़माने के शीर्ष हिंदी दैनिक के लखनऊ,जयपुर और प्रमुख दिल्ली संस्करणों को निकाला है. उनकी सारी फ़ाइलें उपलब्ध हैं. हिंदी पत्रकारिता दो-एक अपवादों को छोड़ कर तब भी पेशेवर और नैतिक रूप से मंझोले दर्ज़े की थी,आज तो वह कुल मिलाकर औसत से भी नीचे है. आज जब पूरे अख़बार ही ‘विज्ञापकीय’ बनने की फिरंगी थर्ड-पेज दिशा में दौड़ रहे हों – जबकि पश्चिम में इतनी निर्लज्जता अकल्पनीय है – तो ‘पत्रकारिता’ शब्द ही ‘टैग’, ‘लेबल’ और ‘ब्रांड’ बन चुका है.
आज अख़बार आदर और प्रतिष्ठा के अलावा सबकुछ कमा रहे हैं. मैं नहीं समझता कि प्रबंधन की प्रबुद्ध जन-प्रतिबद्धता के बगैर मौजूदा अखबारनवीसी की दशा-दिशा बदल पाएगी.मुझे दैनिकों की प्रिंट-लाइन पढ़ कर हँसना-रोना आता है – जिस बेचारे को ख़बरों के लिए रोज़ कानूनन ज़िम्मेदार घोषित किया जाता है उसी का कोई हाथ अख़बार निकालने में नहीं होता. दशा-दिशा हर शाम किन्हीं अलग सत्ता-केन्द्रों से तय होती है.
आज फिल्मों की चर्चा बस उनकी कमाई तक केन्द्रित होती दिखती है. उनके कला-पक्ष पर कोई बात नहीं करता. 'बाहुबली’, 'दंगल’ और ‘हिंदी मीडियम’ जैसी फिल्मों को प्रचार से अलग आप किस तरह देखते हैं?
जबसे फ़िल्में बन रहीं हैं तब से बॉक्स-ऑफिस श्वान-देवी का मंदिर है. संसार के महानतम निर्माता-निदेशक भी चाहते हैं कि उनके कला-पक्ष पर तो बात हो, दर्शक कलदार-पक्ष की बात भी करें. सब जानते हैं कि ‘बाहुबली’ एक विकल-मस्तिष्क फ़िल्म है जिसने चीन को भी क़ायल कर अब तक 1500 करोड़ का बिज़नेस कर लिया है. लेकिन हम अपने बड़े कवि रघुवीर सहाय के वज़न पर कह सकते हैं कि हे प्रभु यह तेरी दया नहीं तो क्या है कि ‘दंगल’ और ‘हिंदी मीडियम’ जैसी ‘बेहतर’,’सोद्देश्य’ फ़िल्में भी आख़िर चल ही गईं.
मेरे लिए दिलचस्प यह जानना है कि इन तीनों फिल्मों के ‘कॉमन’ दर्शक कौन थे, वह क्या सोच कर तीनों को या ऐसी दूसरी फिल्मों को, देख लेते हैं – एन्जॉय करने में शर्मिदा नहीं होते? क्या ख़ुद हम उनका या अन्य ऐसी ही विदेशी फिल्मों का लुत्फ़ नहीं उठाते? भारतीय दर्शकों की पेंचीदा, उदार फ़िल्म-रुचि का व्यापक विश्लेषण तो क्या, एक छोटा सर्वेक्षण तक नहीं हुआ है.